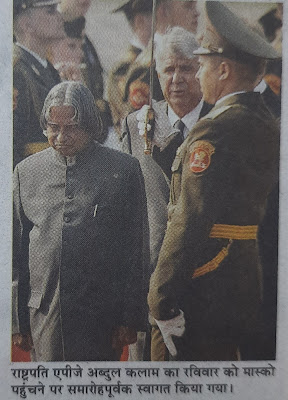राजनीति के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का तमाचा
जयशंकर गुप्त
https://youtu.be/pdxZu1ANxLcराजनीति का तेजी से हो रहा अपराधीकरण पिछले कई दशकों से भारतीय राजनीति और हमारे संसदीय लोकतंत्र को भी डंसे जा रहा है. बार-बार की चेतावनियों और घोषणाओं के बेअसर रहने के बाद अभी एक बार फिर हमारी सर्वोच्च अदालत ने राजनीति के अपराधीकरण या कहें अपराध के राजनीतिकरण पर गहरी चिंता व्यक्त की है. सुप्रीम कोर्ट की राय में “राजनीतिक व्यवस्था की शुद्धता के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को कानून निर्माता बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.’’
वाकई, हाल के दशकों में भारतीय राजनीति और हमारी चुनाव प्रणाली में जाति, धर्म, धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल बढ़ा है. यह हमारी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए अशुभ संकेत है. सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि कुछेक अपवादों को छोड़ दें तो यह किसी भी राजनीतिक दल और आम जनता के लिए भी विशेष चिंता का विषय नहीं रह गया है. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जानेवाले भारत में चुनाव सुधारों की बात तो लंबे समय से होती रही है. लेकिन, आजादी के 74 साल बाद भी यहां 'राजनीति के अपराधीकरण' पर रोक नहीं लग सकी है. भारतीय स्वतंत्रता के 75वें दिवस का जश्न मनाते समय क्या यह हमारी सामूहिक चिंता का विषय नहीं होना चाहिए कि सत्रहवीं लोकसभा के तकरीबन 43 प्रतिशत सदस्यों पर आपराधिक और इन में से 29 प्रतिशत सांसदों पर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं.
मोदी से जगी थी उम्मीद !
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद उम्मीद बढ़ी थी कि अब राजनीति अपराधियों से मुक्त हो सकेगी. हालांकि गुजरात में मुख्यमंत्री रहते ऐसा कुछ भी लहीं किया था जिससे अपराधी राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर हो सकें. लेकिन उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही भाजपा ने जब 7 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने चुनाव घोषणापत्र या कहें संकल्प पत्र में अपराधियों को राजनीति से बाहर करने के लिए कटिबद्धता जाहिर की, तो आस जगी थी. यही नहीं मोदी जी ने खुद भी राजस्थान में अपने चुनावी भाषणों में कहा था, ‘‘आजकल यह चर्चा जोरों पर है कि अपराधियों को राजनीति में घुसने से कैसे रोका जाए. मेरे पास इसका एक ठोस इलाज है. मैंने भारतीय राजनीति को साफ करने का फैसला कर लिया है. मैं इस बात को लेकर आशान्वित हूं कि हमारे शासन के पांच सालों बाद पूरी राजनीतिक व्यवस्था साफ-सुधरी हो जाएगी और सभी अपराधी जेल में होंगे. इस मामले में कोई भेदभाव नहीं होगा और मैं अपनी पार्टी के दोषियों को भी सजा दिलाने में संकोच नहीं करूंगा.’’
 |
| नरेंद्र मोदीः राजनीति के अपराधीकरण का इलाज है, मेरे पास! |
लेकिन प्रधामंत्री मोदी की इन घोषणाओं का हुआ क्या ! इसे भी देखें. 2014 के लोकसभा चुनाव में जीते भाजपा के 282 सांसदों में से 35 फीसदी (98) सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे. इनमें से 22 फीसदी सांसदों के खिलाफ तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे. इन्हें उम्मीदवार किसने और क्यों बनाया था ! यह भी क्या कोई पूछने की बात है ! यही नहीं, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में भी 31 फीसदी सदस्यों के विरुद्ध आपराधिक और इनमें से 18 फीसदी यानी 14 मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे. इन्हें ठोक बजाकर मंत्री भी तो मोदी जी ने ही बनाया होगा ! 14 दिसंबर 2017 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया था कि उस समय 1581 सांसद व विधायकों पर करीब 13500 आपराधिक मामले लंबित हैं और इन मामलों के निपटारे के लिए 12 विशेष अदालतों का गठन होगा. इसके तीन महीने बाद, 12 मार्च 2018 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश के 1,765 सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. जाहिर सी बात है कि भाजपा और मोदी जी ने भी राजनीति को अपराध मुक्त बनाने के जो वादे और दावे किए थे, वह भी उनके सत्ता संभालने के सवा सात साल बाद भी पूरा होने के बजाय कोरा जुमला ही साबित हुए. इस दौरान उनकी पार्टी के कई सांसदों, मंत्रियों और विधायकों पर भी कई तरह के अपराध कर्म में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे लेकिन उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की बात तो दूर, उन्होंने सामान्य नैतिकता के आधार पर किसी का इस्तीफ़ा तक नहीं लिया.
 |
| सुप्रीम कोर्टः राजनीतिक व्यवस्था के अपराधीकरण का खतरा |
हाईकोर्ट की अनुमति के बिना जन प्रतिनिधियों के मुकदमों की वापसी नहीं !
 |
| चीफ जस्टिस एन वी रमनः माननीयों पर मुकदमों की वापसी के लिए हाईकोर्ट की अनुमति जरूरी |
सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों के बाद कहा जा सकता है कि अपराधी छवि वाले नेताओं के लिए चुनाव लड़ने और राजनीतिक दलों को उन्हें उम्मीदवार बनाने में मुश्किलें होंगी. लेकिन क्या इससे राजनीति में अपराधीकरण पर रोक भी लग सकेगी! दरअसल, दशकों पहले से राजनीति के अपराधीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें अपराधियों का राजनीतिकरण अब आम बात हो गई है. पांच दशक पहले तक राजनीतिक दल और उनके नेता चुनाव जीतने के लिए अपराधियों, बाहुबलियों और धनबलियों का इस्तेमाल करते थे. बाद में जब इन लोगों को लगा कि वे किसी को चुनाव जिता सकते हैं तो खुद भी तो जीत सकते हैं. इसी सोच के तहत 1980 में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में तकरीबन डेढ़ दर्जन दुर्दांत अपराधी निर्दलीय चुनाव जीत कर आए. बाद में तकरीबन सभी उस समय के सत्तारूढ़ दल, कांग्रेस में शामिल हो गए. बिहार प्रवास के दौरान मुझे उस समय का एक मजेदार किस्सा सुनने को मिला. एक चुनावबाज नेता जी ने अपने सहयोगी रहे एक बड़े अपराधी को पत्र लिखा कि इस बार फिर वह चुनाव लड़ रहे हैं. पिछली बार की तरह इस बार भी चुनाव में उनकी जरूरत पड़ेगी. लिहाजा, हरबा- हथियार और गुर्गे लेकर उनके चुनाव क्षेत्र में पहुंच जाएं. उधर से जवाब आया, भाई जी, इस बार तो हम खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं. नतीजा ! अपराधी जीत गया और नेता जी चुनाव हार गए.
एक समय था जब भ्रष्ट, सांप्रदायिक और अपराधी छवि के लोगों का समाज में हेय या कहें नफरत की निगाह से देखा जाता था. उनके चुनाव लड़ने की बात तो दूर, उनके साथ जुड़ाव भी शर्मिंदगी का कारण बनता था. लेकिन हाल के दशकों में इस तरह के लोगों की सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ी है. भ्रष्ट और अपराधी छवि के लोगों-नेताओं को उनकी जाति और धर्म के लोगों का भरपूर साथ मिलने लगा है. अब इसे उनका डर कहें या उनके पैसों और बाहुबल का प्रभाव, ये लोग किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होकर या निर्दलीय चुनाव लड़कर भी आसानी से जीत जाते हैं. इस दौरान इन पर लगे आपराधिक मामलों के बारे में लोग कतई नहीं सोचते हैं. राजनीति में वोटों की गलाकाट प्रतिस्पर्धा में सियासी दलों के बीच आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को अपने पाले में लाने की होड़ सी लगी रहती है. राजनीतिक दलों में इस बात की प्रतिस्पर्धा रहती है कि किस दल में कितने उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, क्योंकि इससे उनके चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है. यह भी एक कारण है कि भारत के बड़े हिस्सों में चुनावी राजनीति के मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मूलभूत सुविधाएं न होकर जाति और धर्म होने लगे हैं. इसकी वजह से इन भ्रष्ट और आपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं की जीत आसान हो जाती है. चुनाव जीतने के बाद ये लोग अपने समर्थकों और विरोधियों का 'ध्यान' भी रखते हैं.
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए फैसले और टिप्पणियां करते रहा है. 2002 में सभी तरह के चुनाव में उम्मीदवारों को उनकी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि की घोषणा को अनिवार्य बनाया गया. 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने दो साल से ज्यादा कारावास की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी. 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराए गए, सांसदों और विधायकों को उनके पद पर बने रहने की अनुमति के खिलाफ फैसला सुनाया था. इसी साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईवीएम में नोटा का बटन भी जोड़ा गया था. ताकि मतदाताओं को अगर एक भी उम्मीदवार पसंद नहीं हों तो वे नोटा (यानी कोई नहीं) का बटन दबाकर अपनी नपसंदगी जाहिर कर सकते हैं. लेकिन यह उपाय भी ठोस और कारगर साबित नहीं हो सका क्योंकि इसके जरिए मतदाता अपना आक्रोश और नापंसदगी तो व्यक्त कर सकते हैं लेकिन चुनावी नतीजे को प्रभावित नहीं कर सकते. 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से गंभीर अपराध के आरोपों वाले नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने की सिफारिश की थी. 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जन-प्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष अदालतों के गठन का आदेश दिया था. कुछ राज्यों में त्वरित अदालतें गठित भी हुईं लेकिन नतीजा क्इया निकला!
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं. वह राज्य की विधायिका के कार्यों पर सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. दागी उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाने या उन्हें टिकट नहीं देने का निर्णय राजनीतिक दलों को और उन्हें जिताने-हराने का काम मतदाताओं को करना होता है. अगर राजनीतिक दल इस मामले में अपनी ओर से कोई पहल नहीं करें तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है ! लिहाजा हमारे राजनीतिक दलों को ही एक राय से गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को राजनीति से परे रखने के लिए इस दिशा में ठोस पहल करने के साथ ही संसद से कड़ा कानून भी बनाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि संसद से कानून बनाकर आपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं को राजनीति में आने से रोका जाना चाहिए. अभी जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 दोषी और दो वर्ष या उससे अधिक की सजा प्राप्त राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है. लेकिन ऐसे नेता जिन पर कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर लगे आरोप कितने गंभीर हैं. लेकिन कई बार बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेता-कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक विरोध, धरना, प्रदर्शन और आंदोलन के क्रम में तथा आंदोलन के दौरान यदा-कदा हुई हिंसक घटनाओं को लेकर भी मुकदमे दर्ज होते रहते हैं. उनका क्या होगा. इस पर भी हमारी सर्वोच्च अदालत, संसद और अन्य संबद्ध संस्थाओं को विचार करने की आवश्यकता है. आजादी के 74 साल बाद भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था गंभीर प्रवृत्ति के अपराधियों और राजनीतिक आंदोलनों में निरुद्ध होनेवाले लोगों में फर्क नहीं कर सकी है. अंग्रेजों के जमाने से ही राजनीतिक धरना, प्रदर्शन और आंदोलन में शामिल लोगों को भी अपराध की उन्हीं धाराओं में निरुद्ध किया जाता है जिनके तहत गंभीर किस्म के अपराधियों पर मुकदमें दर्ज होते हैं. राजनीतिक विरोध, धरना, प्रदर्शन और आंदोलन से जुड़े मामलों को अपराध की सामान्य परिभाषा से अलग करने पर विचार करना होगा.
बहरहाल, क्या हमारी सरकार और हमारे राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के आदेश-निर्देशों के अनुरूप इस मामले में कोई ठोस पहल करेंगे ! दरअसल, सभी दल चुनाव सुधारों की बात तो जोर शोर से करते हैं लेकिन मौका मिलते ही अपनी चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए उन सभी बुराइयों का लाभ लेने में जुट जाते हैं जिनका चुनाव सुधारों के क्रम में निषेध आवश्यक है. यह आश्चर्यजनक नहीं है कि डेढ़ साल पहले भाजपा और मोदी जी अपने घोषणापत्र से लेकर भाषणों में भी राजनीति को अपराधमुक्त करने का जो नारा देते थे, 2019 के लोकसभा चुनाव के समय उसे वे भूल ही गए. मोदी जी के चुनावी भाषणों और भाजपा के घोषणापत्र से भी राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाने की बात गायब हो गई.